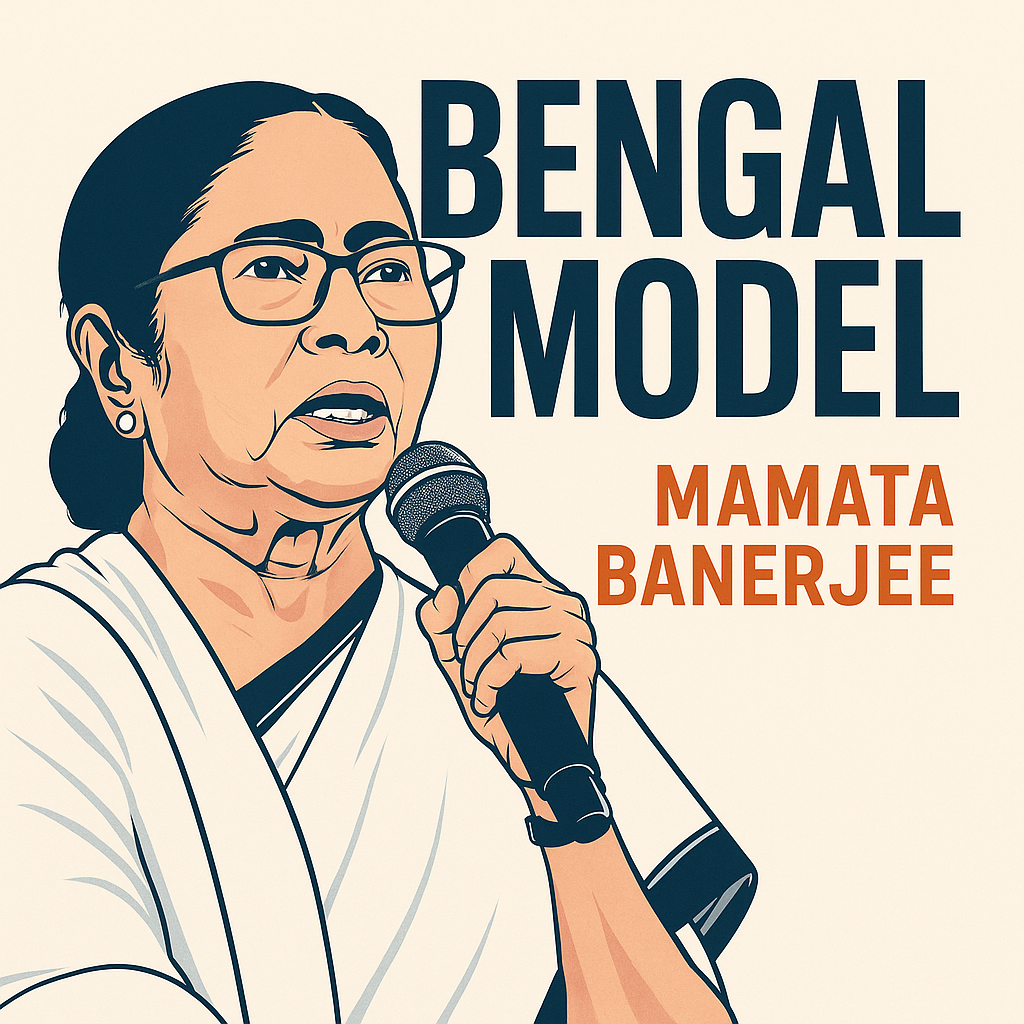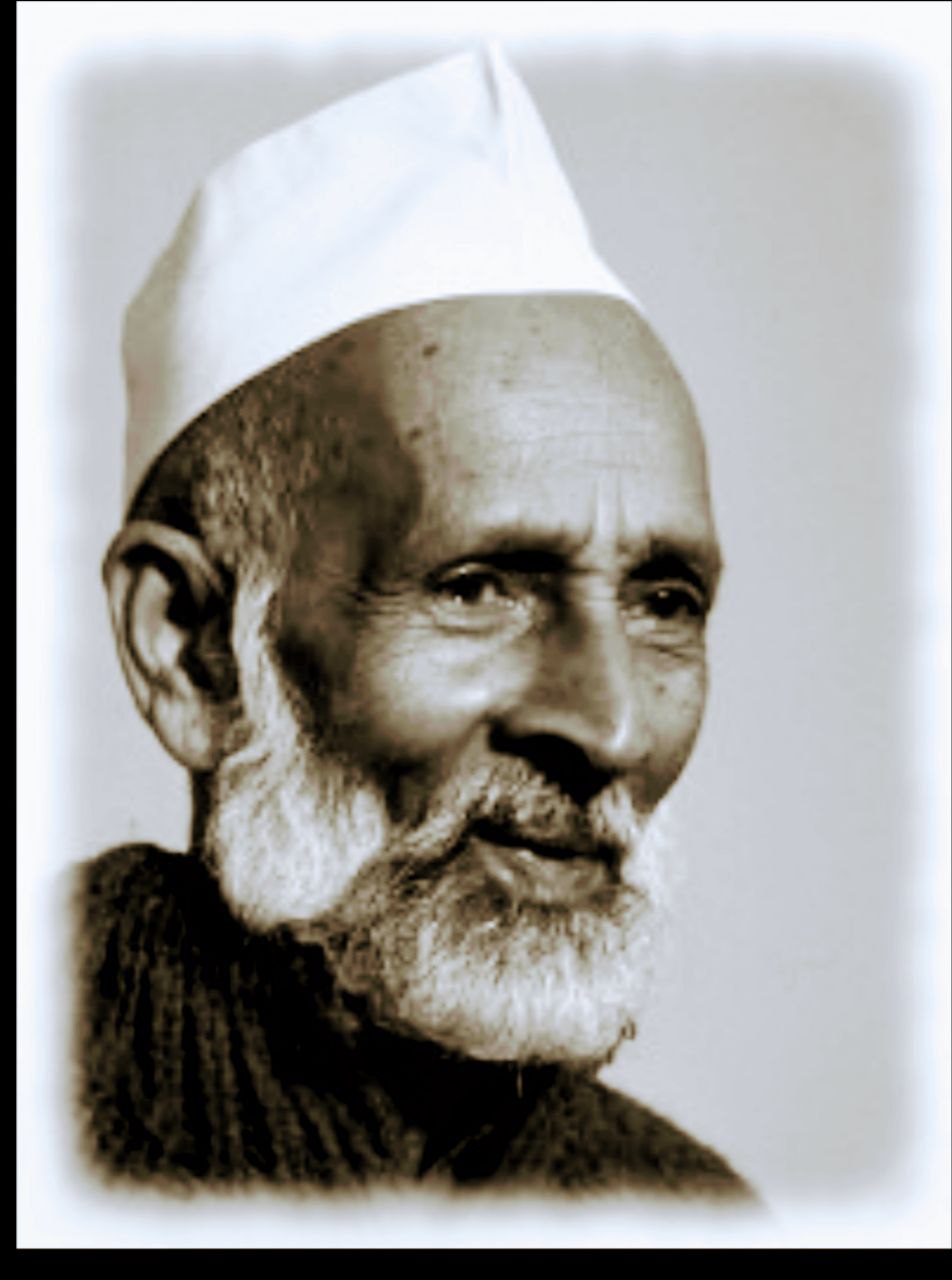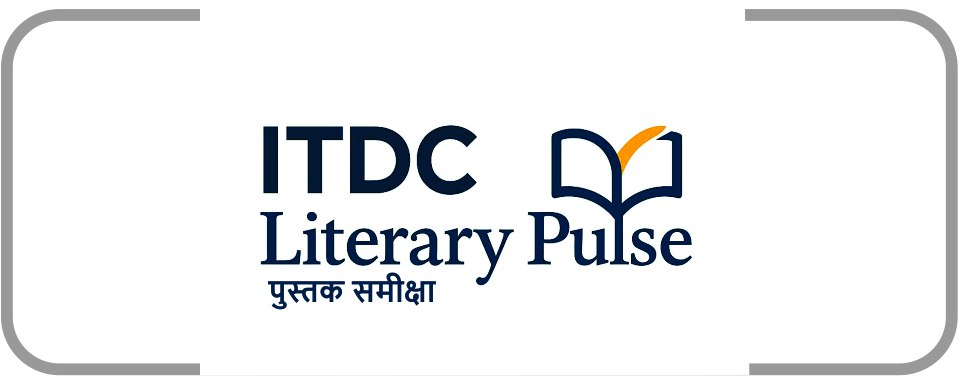अप्रैल 2025 में जाति-आधारित जनगणना की माँग भारतीय राजनीति और समाज में एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन चुकी है। विशेष रूप से बिहार और कर्नाटक के जाति-आधारित सर्वेक्षणों ने इस बहस को नई गति दी है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर अनिश्चितता बनी हुई है, और यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जटिल बना हुआ है। इस एडिटोरियल में हम जाति-आधारित जनगणना की प्रगति, चुनौतियाँ, और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे।
- प्रगति और राज्य-स्तरीय पहल
जाति-आधारित जनगणना को लेकर राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं:
बिहार ने 2023 में अपनी जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें यह पाया गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मिलकर राज्य की 63.14% आबादी का हिस्सा हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम ने नीतिगत बदलावों, जैसे आरक्षण सीमा बढ़ाने की माँग को बल दिया।
कर्नाटक ने 2015 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को 2024-25 में नवीनीकरण किया, जिसमें 6.6 करोड़ लोगों का डेटा शामिल किया गया।
अन्य राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा, और तमिलनाडु ने भी जातिगत डेटा संग्रह के लिए विधायी प्रस्ताव पारित किए हैं।
उत्तर प्रदेश में इस विषय पर सिर्फ राजनीतिक माँगें उठी हैं, जैसे कि सपा का 2022 घोषणापत्र, लेकिन इसके आगे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
- केंद्र सरकार पर दबाव
केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
गृह मंत्रालय ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जाति जनगणना “प्रशासनिक रूप से कठिन” है, क्योंकि 2011 के SECC में 46 लाख जाति श्रेणियाँ दर्ज की गईं, जिनमें 81.9 मिलियन त्रुटियाँ थीं।
सरकार सामाजिक विभाजन और डेटा की विश्वसनीयता की चिंताओं का हवाला देती है।
BJP खासकर ओबीसी-प्रधान राज्यों में उच्च जातियों के विरोध और चुनावी जोखिमों के कारण सतर्क है।
- सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सर्वेक्षण को 2023 में वैध ठहराया, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा पर अभी तक कोई नया फैसला नहीं आया है।
कांग्रेस ने अक्टूबर 2023 में CWC प्रस्ताव के माध्यम से जाति जनगणना का वादा किया, और विपक्षी नेता इसे “आर्थिक और सामाजिक न्याय” के तौर पर पेश कर रहे हैं।
तमिलनाडु ने 2024 में केंद्र से जाति जनगणना की माँग की, लेकिन स्वतंत्र सर्वेक्षण से इनकार किया, क्योंकि केवल केंद्र ही Census Act, 1948 के तहत इसे कर सकता है।
- जातिगत डेटा की आवश्यकता और साक्षात्कार
जातिगत डेटा की आवश्यकता को NFHS-5 (2019-21) जैसे सर्वेक्षणों से समझा जा सकता है। ये सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि SC/ST महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 59% है, जबकि सामान्य वर्ग में यह 80% है। इसके अलावा, ग्रामीण OBC कृषि मजदूरों की औसत आय (₹1.2 लाख/वर्ष) सामान्य वर्ग के किसानों (₹3.5 लाख/वर्ष) से काफी कम है।
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत डेटा की आवश्यकता है, ताकि उचित नीतियाँ बनाई जा सकें।
- आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
जातिगत डेटा को लेकर आलोचनाएँ भी उठाई जा रही हैं:
कुछ आलोचक मानते हैं कि जातिगत डेटा राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहसें हो रही हैं, जैसे X पर BJP-RSS के डर के दावे
पारदर्शी दिशानिर्देशों और डेटा गोपनीयता की कमी के कारण सर्वेक्षण में अविश्वास पैदा हो सकता है।
तकनीकी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे 3.3 मिलियन गणनाकर्ताओं का प्रशिक्षण, डिजिटल ऐप्स (जैसे बिहार का Bijaga), और सांख्यिकी आयोग के साथ समन्वय।
- 2025 की संभावनाएँ
राष्ट्रीय जाति जनगणना की घोषणा 2025 में संभव है, लेकिन कार्यान्वयन 2026 से पहले मुश्किल हो सकता है।
केंद्र को राज्यों, सांख्यिकी आयोग, और समाजशास्त्रियों के साथ मिलकर फील्ड-वर्क प्रोटोकॉल तैयार करना होगा।
डेटा को आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, और भूमि स्वामित्व जैसे मानकों के साथ जोड़ना होगा।
- जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार बनने से रोकना
जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार बनने से रोकने के लिए पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है।
यदि भारत इस दिशा में सही कदम उठाता है, तो जाति जनगणना सामाजिक न्याय और नीति-निर्माण के लिए ठोस आधार बन सकती है, जो दशकों तक असमानताओं को कम करने में मदद करेगा।
निष्कर्ष:
जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता को लेकर भारत में गहरी बहस चल रही है। इसके लिए समर्पित राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि यह सर्वेक्षण सामाजिक न्याय और विकास में सहायक हो सके। यदि इसे सही दिशा में चलाया गया, तो यह न केवल असमानताओं को उजागर करेगा, बल्कि भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा।
#जाति_आधारित_जनगणना #जाति_सर्वेक्षण #जातिगत_डेटा #समाज #भारत #राजनीति #आर्थिक_न्याय